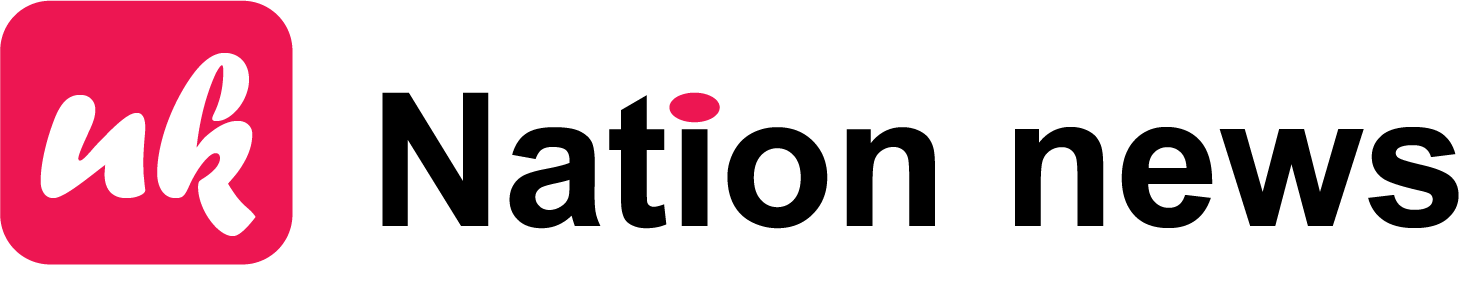सशक्त भूमि अधिनियम और 1950 को आवासीय प्रमाण के लिए आधार वर्ष बनाने की मांग को लेकर देहरादून में एक विशाल रैली के बाद दिल्ली में उत्तराखंड के रेजिडेंट कमिश्नर के सामने विरोध प्रदर्शन



दिल्ली में उत्तराखंड के कई सामाजिक राजनीतिक संगठनों और उत्तराखंड के पत्रकारों, लेखकों और विचारकों सहित उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने आज राष्ट्रीय राजधानी में कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया और पिछले तीन दिनों से सूरज नहीं निकलने के बावजूद पूरे समर्पण के साथ अपनी मांगों को लेकर नारे लगाए। उत्तराखंड में आवासीय प्रमाण के लिए आधार वर्ष के रूप में उत्तराखंड का कंक्रीट भूमि अधिनियम, 1950, कई पूर्वोत्तर राज्यों की तरह अनुच्छेद 371 का कार्यान्वयन और मौजूदा कानून को समाप्त करना जिसने 12.5 एकड़ भूमि की सीमा को हटा दिया है। कुछ उद्योग आदि खोलने की आड़ में कृषि और अन्य भूमि बाहरी लोगों द्वारा बेची और खरीदी गई।

नई दिल्ली के आईटीओ के पास राउज एवेन्यू में उत्तराखंड के रेजिडेंट कमिश्नर के कार्यालय के बाहर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न स्थानों से लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर स्थानिक आयुक्त को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया।

कृपया याद करें कि अभी कुछ दिन पहले इन्हीं मांगों को लेकर देहरादून में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था जिसमें देश के कोने-कोने से हजारों पूर्व सैनिकों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और यहां तक कि वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया था और हाथों में प्ले कार्ड लेकर कई किलोमीटर तक मार्च किया था। उनके हाथों में ठोस भूमि अधिनियम और उत्तराखंड के निवासियों को आवासीय प्रमाण पत्र देने के लिए 1950 को आधार वर्ष बनाने की मांग करते हुए भाजपा सरकार विरोधी नारे लगाए गए।
दिल्ली में इस अवसर पर उत्तराखंड के एक विश्वसनीय थिंक टैंक चारु तिवारी और आमतौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामाजिक कार्यों में देखे जाने वाले कई जाने-माने चेहरे मौजूद थे।

इस मांग के बारे में ध्यान देने योग्य बात यह है कि कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोग पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ उपरोक्त मांगों के समर्थन में प्ले कार्ड लेकर नारे लगा रहे थे।
उत्तराखंड में पिछले कई वर्षों से ‘मूल निवास’ को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। कोविड के बाद जब लोग अपने गांव वापस जाने लगे तो राज्य गठन के बाद पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं. वह उन्हें नए सिरे से जानने की कोशिश करने लगा. ‘मूल निवास’ भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य को दिया गया एक संवैधानिक प्रावधान है, जो उस राज्य का मूल नागरिक होने का अधिकार देता है। इस अधिकार के साथ वह उन सभी सुविधाओं और अवसरों का पहला हकदार है जो सरकारें समय-समय पर वहां के लोगों को प्रदान करती हैं।

लेकिन, पहली अंतरिम सरकार से लेकर आज तक चुनी गई सरकारों ने उत्तराखंड में इन सुविधाओं को बढ़ाने के बजाय इन्हें खत्म करने का काम किया। इस आंदोलन की मांग है कि उत्तराखंड में 1950 की मूल निवास सीमा लागू की जाये.
उत्तराखंड के लोगों की यह मांग अप्रत्याशित नहीं है। हमारे देश में 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही यह प्रावधान किया गया कि जो व्यक्ति संविधान लागू होने के वर्ष यानी 1950 में जिस राज्य में रह रहा था, उसे उस राज्य का मूल निवासी माना जाएगा। इसके लिए देश की राष्ट्रपति अधिसूचना जारी की गई थी.
इस प्रावधान को 1961 में राष्ट्रपति द्वारा फिर से अधिसूचित किया गया क्योंकि साठ के दशक में अधिक राज्यों का गठन किया गया था। इस अधिसूचना के आधार पर आरक्षण और अन्य योजनाएँ शुरू की गईं जिनका लाभ उस राज्य के मूल निवासी उठा सकते थे। यह फिलहाल देशभर के हर राज्य में लागू है।

राज्य के गठन के बाद जब नित्यानंद स्वामी के नेतृत्व में पहली अंतरिम सरकार बनी तो उसने यहां के निवासियों को ‘मूल निवासी’ मानने से इनकार कर दिया. इस सरकार ने ‘मूल निवासी’ और ‘स्थायी निवासी’ को एक ही माना और इसकी कट ऑफ डेट 1985 तय की। इसके बाद राज्य में ‘मूल निवास’ के बजाय ‘स्थायी निवास’ की व्यवस्था लागू हो गई। इससे यहां के निवासियों के अधिकारों पर हमला हुआ. कट ऑफ डेट 1985 होने के कारण बड़ी संख्या में वे लोग भी स्थानीय अधिकारों के हकदार बन गये जो 15 साल पहले राज्य में रह रहे थे.
उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद लगातार मूल निवास को 1950 में बदलने की मांग उठती रही। इस मामले में एक अच्छा संकेत 2010 में मिला जब मूल निवास से संबंधित एक याचिका पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने एकल अधिवास यानी मूल निवासी की व्यवस्था को जारी रखते हुए 1950 की राष्ट्रपति अधिसूचना को उत्तराखंड में भी बरकरार रखा। देश में निवास.
उस समय उत्तराखंड हाई कोर्ट में ‘नैना सैनी बनाम उत्तराखंड राज्य’ और सुप्रीम कोर्ट में ‘प्रदीप जैन बनाम भारत सरकार’ की दो अलग-अलग याचिकाओं में कहा गया था कि जो व्यक्ति उत्तराखंड राज्य के गठन के समय यहां रह रहा था. को मूल निवासी माना जाना चाहिए, लेकिन दोनों अदालतों ने इसे नहीं माना और 1950 के प्रावधान को लागू रखा।
यह फैसला उत्तराखंड के नागरिकों के लिए बड़ी राहत था, लेकिन 2012 में इसी मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि जो भी व्यक्ति 9 नवंबर 2000 को यानी कि उत्तराखंड का नागरिक था. राज्य गठन के दिन, सीमा के भीतर रहने वाला कोई भी व्यक्ति यहां का मूल निवासी माना जाएगा। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उस निर्णय को स्वीकार कर लिया। सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ वह न तो हाई कोर्ट गईं और न ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
हालांकि, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले के आलोक में 2010 से ही इस मुद्दे को खत्म करने की योजना बनायी थी. बाद में 2012 में राज्य गठन के लिए कट ऑफ डेट यानी 2000 तय करने के एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर की गई, लेकिन तत्कालीन सरकार ने ऐसा नहीं किया।
यह चुनौती इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि यह फैसला राष्ट्रपति अधिसूचना के अधिनियम-5 और 6 की अनुसूची के साथ-साथ ‘उत्तराखंड राज्य पुनर्गठन अधिनियम-2000’ की धारा 24 और 25 का उल्लंघन था। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और राज्य में स्थायी निवास की व्यवस्था पूरी तरह से लागू कर दी गयी.
इसके लागू होने से यहां के निवासियों का स्थानीय संसाधनों पर अधिकार और समय-समय पर सरकारों द्वारा दी जाने वाली रियायतें सीमित हो गयीं, क्योंकि 1985 की कट ऑफ डेट के बाद बड़ी संख्या में वे अधिकार पाने के हकदार भी बन गये. स्थायी निवासियों से. जो 1985 या 2000 से उत्तराखंड में रह रहे हैं। पहले से ही पलायन की मार झेल रहे उत्तराखंड जैसे सीमित अवसरों वाले राज्य के लिए यह अपने अस्तित्व को बचाने के सवाल से जुड़ गया है।
इसी प्रकार, उत्तराखंड के कंक्रीट भूमि अधिनियम के संदर्भ में, उत्तराखंड के लिए सबसे चिंताजनक बात यह है कि सरकारों के जनविरोधी भूमि कानूनों के कारण राज्य में खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा है। वर्तमान में राज्य की केवल 4 प्रतिशत भूमि पर ही खेती की जा रही है। हमारे पास अधिकतम 6 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि बची है। राज्य में कुल भूमि क्षेत्र का 63 प्रतिशत वन है, 14 प्रतिशत कृषि है, 18 प्रतिशत बंजर भूमि है और 5 प्रतिशत बंजर या अनुपयुक्त भूमि है। अंग्रेजों ने हमारी जमीनें 11 बार नापी थीं। आज़ादी के बाद आख़िरकार 1964 में आंशिक माप किया गया। राष्ट्रीय पार्कों और वन विहारों के विस्तार के कारण लोग अपनी ज़मीन से अलग हो गए हैं। इसलिए हमारी पहली मांग है कि उत्तराखंड में जमीनों की पैमाइश कराकर गलत तरीके से वन विभाग और सरकारी खातों में जमा की गई जमीनों को मुक्त कराकर कृषि भूमि में शामिल किया जाए।
इन चौंकाने वाले आंकड़ों के बावजूद सरकारों ने हमारी जमीनें सीधे बेचने की व्यवस्था कर ली। त्रिवेन्द्र रावत के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 6 दिसंबर, 2018 को विधानसभा में ‘उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (अनुकूलन और संशोधन आदेश 2001) (संशोधन) अध्यादेश -2018’ पेश किया था। एक नये भूमि कानून ने पहाड़ों में भूमि की बड़े पैमाने पर लूट का रास्ता खोल दिया।
इतना ही नहीं नए संशोधन में अधिनियम की धारा 143 के प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया. पहले इस अधिनियम के अनुसार कृषि भूमि को अन्य उपयोग में परिवर्तित करने के लिए राजस्व विभाग की अनुमति आवश्यक होती थी। इस संशोधन के जरिये इस धारा को 143 (ए) में बदल दिया गया. अब हमें अपने उद्योग का प्रस्ताव सरकार से पास कराना है. इसके लिए खरीदी गई कृषि भूमि का भू-उपयोग बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसे बहुत आसानी से गैर कृषि योग्य भूमि मान लिया जाएगा।
इस संशोधन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी भी निवेशक को पहाड़ों में उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीदने की आजादी देता है। इससे आगे बढ़कर सरकार ने इस कानून की धारा 156 में संशोधन कर तीस साल के लिए जमीन पट्टे पर देने का अध्यादेश पारित कर दिया है. इससे समझा जा सकता है कि कृषि के माध्यम से रोजगार देने की बात करने वाली सरकारों के दावे कितने खोखले हैं। इसलिए हमारी मांग है कि 2018 में सरकार द्वारा भूमि कानून में किये गये संशोधन को तुरंत रद्द किया जाये.
उत्तराखंड को छोड़कर देश के अन्य हिमालयी क्षेत्रों की संवेदनशीलता को समझते हुए यहां बहुत सख्त भूमि कानून बनाए गए हैं। जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 और 35-ए (अब हटाए गए) के कारण जमीन की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध था। उत्तर-पूर्वी राज्यों में धारा 371 के माध्यम से जमीनों को बचाया गया है। हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में ‘हिमाचल प्रदेश टेनेसी और भूमि सुधार अधिनियम-1972’ के अध्याय 11 में ‘भूमि हस्तांतरण पर नियंत्रण’ में धारा 118 है।
इस धारा के अनुसार हिमाचल में किसी भी गैर कृषक को भूमि हस्तांतरित नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह भी है कि हिमाचल का निवासी कोई गैर-किसान भी कोई कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। इसी धारा 38-ए की धारा 3 में यह भी कहा गया है कि कोई भी भारतीय (गैर-हिमाचली) आवासीय भूमि खरीदने के लिए आवेदन कर सकता है। इसकी सीमा भी 500 वर्ग मीटर होगी. लेकिन इसके लिए भी सरकार से इजाजत लेनी होगी. यदि गैर हिमाचली सरकारी कर्मचारी भी अपना आवास बनाना चाहते हैं तो उनके पास भी हिमाचल में तीस साल की सरकारी सेवा का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
सिक्किम के ‘सिक्किम रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा 3 (ए) में यह प्रावधान किया गया है कि केवल लिम्बु या तमांग समुदाय में ही जमीन खरीदी या बेची जा सकती है। यह प्रावधान भी किया गया है कि जमीन बेचने वाले को कम से कम तीन एकड़ जमीन अपने पास रखनी होगी. यह प्रावधान इसलिए किया गया ताकि जमीन बेचने वाला व्यक्ति भूमिहीन न रहे.
इन संक्षिप्त आंकड़ों और मौजूदा कानूनों से हम समझ सकते हैं कि कैसे उत्तराखंड के लोगों को उनकी जमीन से अलग करने की साजिशें की गई हैं। अगर समय रहते इसका मुकाबला नहीं किया गया तो हमारे सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। इन सभी चिंताओं को लेकर पिछले कुछ दिनों में पूरे उत्तराखंड में युवाओं के बीच से जो विरोध की गूंज उठी है, उसका असर उन प्रवासियों पर पड़ना तय है, जो पलायन की त्रासदी से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं।