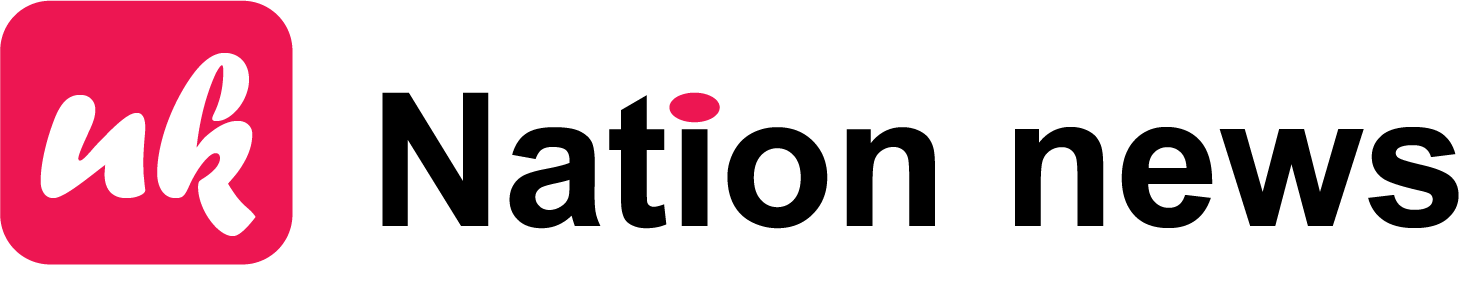सुन भई उत्तराखण्ड!
मां को लेकर किधर जाएं हम?

वरिष्ठ साहित्यकार नरेंद्र कठैत
ऐसा नहीं कि पहले नहीं लिखा। लिखा था पर आपने सुना ही नहीं। आपने भी तो कहा था कि अलग राज्य बनेगा तो यहां की कला,साहित्य, संस्कृति का विकास आपकी प्राथमिकता में होगी। हमें खूब याद है वह दिन जब पहली बार गांव की पगडण्डी सड़क तक पहुंची थी -और सबसे पहले वहां चाय की दुकान खुली थी। कला,साहित्य,संस्कृति की चर्चा भी सबसे पहले हमनें वहीं सुनी थी। पहल अच्छी थी- आगे विकास की सम्भावनाएं भी थी।
लेकिन बड़े अरमानों के साथ खोली गई उस दुकान की रौनक धीरे-धीरे कम होती गई। वह इसलिए-क्योंकि-उसी दुकान के समीप एक अन्य भाई ने भी चाय की दुकान खोल दी थी। और फिर- जो बात होनी थी वहीं हुई। लोगों ने दोनों के बीच सुलह समझौते की कोशिश भी की। किन्तु दोनों के बीच कलह जो एक बार बढ़ी वह फिर रूकी नहीं। थक हार कर सभी ने यही कहा- ‘छोड़ो अपनी केतली की चाय ही भली!’
इसी बीच सुना कि उनके समीप एक भव्य माॅल खुलने जा रहा है। अब उन दोनों की चिन्ता की सुई माॅल की ओर सरक गई है। एक कहता है-‘भैजी! माॅल वाले से पूछ तो लो वह चाय पत्तियां कौन सी कम्पनी की डालेगा- ‘टाटा की,बु्रक बाॅण्ड की या बाघ बकरी?’ दूसरा कहता है-‘अरे दाजू! पानी नाली से उठायेगा- ‘दूध होगा पाउडर का- वह भी मिलावटी! इस माॅल वाले का विरोध होना ही चाहिए जी!’
हमनें कहा -‘भाई! घबराओं नहीं! अभी तो माॅल की नींव भी नहीं पडी। समय आने पर यह भी देखा जायेगा कि माॅल वाले चाय में अदरक डालते हंै कि अरबी? दरअसल -बात यह है भैजी! कि- हमारी चिन्ता का विषय न आपकी चाय है न माॅल वालों की।’
हमारी चिन्ता के मूल में अपनी वे मूल भाषाएं हंै जो आज हमनें ही दोराहे पर खड़ी कर दी। हमनें मूल भाषाओं में वे शब्द घुसेड़ दिये जो आम जनमानस की बोल चाल में कभी रहे ही नहीं। साक्ष्य मौजूद हैं कपोल कल्पित नहीं। उसी खिचड़ी को देखकर यह बात उठी-न गढ़वाली न कुमाऊनी- दोनों को मिलाकर भाषा बनेगी ‘ उत्तराखण्डी’। इसी विचार पर कुछ तलवारें आपने भांजनी शुरू की तो कुछ उन्होंने भी भांजी! और सवालिया निगाह हमारी ओर डाल दी।
इसी भंजम-भंजाई पर वरिष्ट पत्रकार जगमोहन रौतेला कहते हैं -‘भाई! जब मुखर होना होता है तब हमारी आंखें मूंद जाती है। और दूसरी बात यह है कि जिसको जो मुद्दा जहां दिख रहा है वहीं से उठाने की हमारी प्रवृत्ति बढ़ गई है। पीछे झांकने की किसी को फुर्सत ही नहीं है। कभी सतपाल महाराज के सद्प्रयास से गढ़वाली कुमाऊनी भाषाओं के लिए ‘महापात्रा समिति’ गठित हुई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को भी सौंप दी थी। उसमें क्या है?-और क्या नहीं? उसको जानने की भी किसी ने कोशिश ही नहीं की। भाई कौन नहीं चाहता हमारी भाषा आठवीं अनुसूची तक पहुंचे। लेकिन माननीयों के हाथों में कागज थमाने से पहले पूरे तथ्य तो रखें।’ आपका कथन भी उचित ही है रौतेला जी! असल में जितना झोल इधर है उतना ही उधर भी।
तो सूनो जी! ये पंक्तियां आपके लिए भी हैं और उनके लिए भी।
सबसे पहला सवाल तो यही है कि-‘आप प्रवासी गढ़वाली कुमाऊनी भाषा के सक्रिय रचनाकारों के मध्य से ही अलग भाषा के गठन की बात क्यों उठी? यदि ऐसा नहीं तो गढ़वाली कुमाऊनी भाषा का सम्मिश्रण तैयार करने में तत्पर प्रवासी रचनाकारों की अगवाई क्या कोई भ्रम पैदा नहीं करती? दूसरा यह कि यदि देश दुनिया में अपनी भाषा को पहचान दिलाने की ठानी है तो जिस भाषा में हमनें सांस ली उसमें आपको क्या कमी दिखी? मां के पास अगर चप्पलें नहीं या उसके पास फटी पुरानी धोती है तो क्या मां, मां नहीं रहेगी? आपकी दृष्टि में राज्य की दो प्रमुख भाषाएं प्रतिनिधित्व की हकदार क्यों नहीं? एक बात यह भी कि गढ़वाली कुमाऊनी भाषा में रचित उन रचनाओं का आंकलन आप किस रूप में करते हैं जो आपने ही हमें सौंप दी?
क्या इस तथ्य से डा. हरि सुमन बिष्ट जी अनभिज्ञ हैं कि गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा को आधार मानकर ही दशक भर पूर्व ‘साहित्य एकादमी’ गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषाओं में दो वृहद सम्मेलन आयोजित कर चुकी। यही नहीं गढ़वाली एवं कुमाऊनी भाषा की दो-दो विभूतियाँ ‘साहित्य एकादमी पुरस्कार’ से भी सम्मानित की गई। हमारे कई पद्म श्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक एकादमी सम्मान इन्हीं भाषाओं की भाव भूमि की उपज रही। फिर गढ़वाली कुमाऊनी मातृ भाषाओं को आगे रखने में शंका क्यों है जी?
डा. राजेश्वर उनियाल जी! ‘हलन्त’ के जुलाई 22 के अंक में आपने लिखा- ‘ उत्तराखण्ड राज्य के गठन के बाद उत्तराखण्ड के भाषाविदों के समक्ष ठीक इसी प्रकार प्रश्न खड़ा हुआ है कि यदि हम अपने राज्य हेतु किसी क्षेत्रीय भाषा को लागू करना चाहें, तो गढ़वाली,कुमाऊनी व जौनसारी में से कौन सी भाषा हमारी भाषा प्रतिनिधित्व करेगी?’ अग्रज श्री किन भाषाविदों के समक्ष यह प्रश्न उठा आपने लिखा नहीं। उसी आलेख में आपने गढ़वाली कुमाऊनी को भी 20-22 क्षेत्रीय और 60-65 उप बोलियों में बांटा है। साथ ही आम जन मानस के बीच इनका प्रतिनिधित्व भी 50 प्रतिशत से भी कम आंका है। जबकि सत्यता यह है कि किसी भी मूल रचनाकारों ने मूल भाषाओं को इस दृष्टि से कभी देखा ही नहीं है।
प्रश्न आपसे भी है कि राज्य की सीमा के साथ भाषा कैसे निर्धारित होगी? इतिहास गवाह है कि कभी गढ़वाल की सीमा बड़े भू भाग तक फैली थी -किन्तु बाद में वह टिहरी तक ही रह गई। तो क्या गढ़वाली भाषा भी सिमट गई? भैजी यह वह भाषा है जो न चैरासी करों के नीचे दबी, न बिरही की बाढ़ में बही, न इकावनी-बावनी के अकाल में मरी।
देश काल परिस्थिति के अनुसार राज्य की सीमाएं घट-बढ़ सकती हंै-तो भाषाएं भी क्या सीमा के अनुसार तय होगीं? यदि ऐसा सम्भव है तो भाषायी आधार पर हम भी भू-भाग का प्रस्ताव रख लेते हैं। क्या भाईयों के बीच बंटवारे नहीं होते हैं जी?
आदरेय डा. जालन्धरी जी! आप भी हमारे मध्य सम्मानित रचनाकार हैं। मूल भाषा की आप भी इस्पाती रीढ़ रहे हैं। आपके पास तीव्र मेधा है-इसमें कोई दो राय नहीं। यदि निज भाषा की उन्नति का सवाल हो चर्चा तो कहीं भी हो सकती है दुकान में भी, माॅल में भी, मुम्बई में भी और मद्रास-इम्फाल में भी। लेकिन सबसे पहले हमें अपनी केतलियों में जमा वर्षों पुरानी बेजान चाय की पत्तियां बदलनी होगी। अन्यथा वे बेजान पत्तियां हमारा स्वाद ही नहीं अपितु हमारी बुद्धि को भी कुंद करेंगी।
अग्रज श्री! आप नई भाषा के गठन की मुहिम में अग्रिम पंक्ति में हैं। आपको शुभकामनाएं हैं। लेकिन क्या हम ये समझ लें कि अब आप मां से ऊब चुके हैं। और -उसके प्रति अपनी समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो गये हैं? सत्य बात तो यह है कि जन मानस से बढ़कर न आप हैं और न हम हैं! आइये उन्हीं से पूछते हैं- सुन भई उत्तराखण्ड!
मां को लेकर किधर जाएं हम?