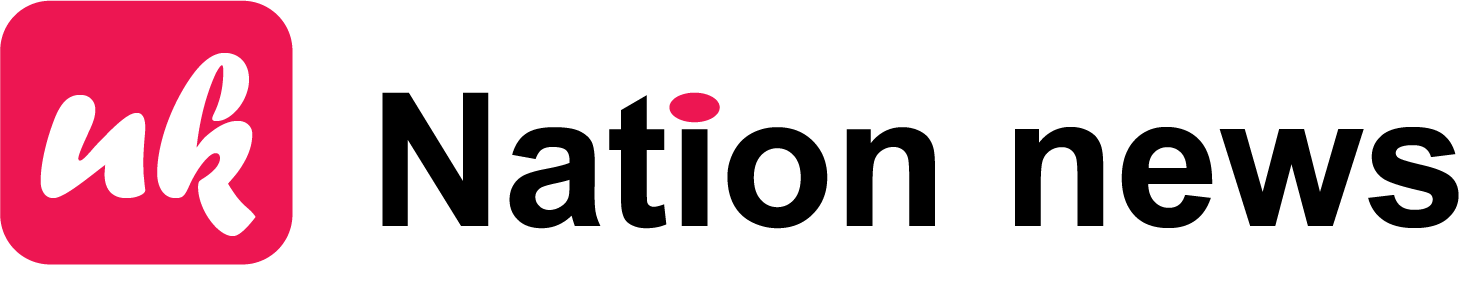विकास मेरे शहर का !गढ़वाल, उत्तराखंड के एक प्रमुख साहित्यकार की नजर में पौडी शहर
पिछली स्याही का और आगे का हिस्सा(भाग तृतीय)


वैसे पहाड़ पर पीठ टिकाए इन शहरों में है भी क्या? सब कुछ चित्र लिखित सा! जैसे मसूरी, वैसे ही नैनीताल! मेरा शहर नगर है, उसे महानगर भी नहीं कह सकता। लेकिन न जाने क्यों किसी भी कैमरे में इस शहर का चौखटा फिट नहीं बैठता । कैमरा आधा शहर पकड़ता, आधा सफाचट कर जाता। लोग आधा शहर देखकर कहते हैं- ‘अरे पौड़ी शहर इतना छोटा सा!’ अब उन्हें कौन समझाए कि ये दोष है सब-कैमरे का! कैमरे की पकड़ में ये आधा आता है, आधा नहीं आता। इसलिए एक कारण ये भी है कि पर्यटक इसे छोटा शहर मानकर भी यहां नहीं आता।
एक बार मेरे एक्टर/होटलीयर मित्र आनन्द कांति ने फोन पर पूछा- ‘पौड़ी के हर एक फोटो में पौड़ी का बस अड्डा दिखता। जैसे किसी किताब का गत्ता! क्या पौड़ी शहर उतना ही है दादा?’ मैंने कहा-‘नहीं पौड़ी शहर बहुत बड़ा है कांति दादा!’ कांति दा ने फिर आगे पूछा-‘फिर हर कोई केवल बस अड्डा ही क्यों दिखाता है? मैंने जवाब दिया-‘दरअसल हमारा यह सोचना है कि उसी बस अड्डे से ‘विकास’ भागा है। इसलिए पौड़ी का नागरिक पौड़ी के बस अड्डे का फोटो हर जगह चस्पा करता है।’
कई लोग पूछते हैं पौड़ी शहर में विशेष क्या है? अब उन्हें क्या बताएं कि पौड़ी शहर में विशेष क्या है? कौन नहीं जानता है कि पौड़ी शहर इधर-उधर के गाँवों के लोगों का जमावाड़ा है! ठीक सामने हिमालय का भाल है लेकिन इस शहर में पानी का सबसे बुरा हाल है। यहां का वाशिंदा – पानी या तो श्रीनगर घाट का या ठेट नानघाट का पीता है। शहर में सब कुछ जैसे उधार का है। किंतु कहावत है- ‘पौड़ी का लाल! उधार का भले ही खाता है लेकिन समय पर कर्ज चुकाता है।’
एक बात और सुनो जी! इसी शहर से जुड़ी दो कहावतें और प्रसिद्ध रही। उनमें से एक यह की- ‘ब्यटा! ऐली त सही, कबि न कबि म्यरि पौड़ी (बेटा! आयेगा तो सही,कभी न कभी मेरी पौड़ी)। ये किसी को डराने धमकाने की मुंह जबानी, तरकीब थी। क्योंकि तब पौड़ी शहर बुद्धिजीवीयो, लेखकों, राजनीतिज्ञों,समाज सेवीयों,संस्कृति कर्मियों का केन्द्र ही नहीें बल्कि दादा टाइप लोगों की भी नर्सरी थी।
लिखते-लिखते एक दादा से जुड़े प्रकरण की याद आ गई। कह नहीं सकता इसमें कितना झूठ का अंश है- और कितनी सच्चाई। लेकिन आग भी कहीं यूं ही नहीं लगती। और अफवाह भी अकारण नहीं फैलती। तो बात हो रही है उन दादा की।
बात ये थी कि…रूको! उससे पहले बात ये हुई कि- व्यंग्य श्रेष्ठ मेरे अग्रज प्रो. राजेश कुमार और मित्र डाॅ. लालित्य ललित ने 63 विशिष्ट व्यंग्यकारों की 63 रचनाओं एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि व्यंग्य संकलन सम्पादित किया है। जिसका नाम है- आँकड़ा तिरेसठ का’! इस पुस्तक में संपादक द्वय ने ‘आँकड़ा तिरेसठ का क्यों नहीं हो सकता’ शीर्षक के अन्तर्गत लिखा है- ‘आपने 36 के आँकड़े के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या कारण है कि 63 का आँकड़ा नहीं हो सकता? हिंदी देवनागरी लिपि में जब हम 36 को अंकों में लिखते हैं, तो वे एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं। इसका अर्थ यह है कि उसमें विपरीत संबन्ध है। और फिर अर्थ का प्रसार होते हुए यह मुहावरा ऐसे व्यक्तियों,समुदायों,राष्ट्रों आदि के संबंध के बारे में यह अर्थ देने लगा कि उनमें विरोध का संबंध है।…तो क्यों नहीं हम तिरेसठ के आँकड़े के बारे में भी बात करें।’ मैंने विस्तार से जानने के लिए व्यंग्यकार मित्र लालित्य ललित से ही जानना चाहा। पूछा- ‘ललित भाई! अमूमन सुनने-पढ़ने में आता है- ‘आँकड़ा छत्तीस का’! आँकड़ा तिरेसठ लिखने के पीछे आपका क्या कोई और कारण भी रहा?’ उन्होंने जवाब दिया- ‘यार आँकड़ा छत्तीस का! अब आम हो गया।
लेकिन हमारे शहर में लगभग छः दशक पूर्व छत्तीस से जुड़ा नाम बदनाम तो हुआ-किंतु उसका नाम न हो सका। सुना है! वो एक स्टाइलिश दादा था। और अपने को कुछ अलग दिखाने के लिए कुछ न कुछ नई तरकीब सोचता रहता था। एक बार वो किसी दर्जी के पास कमीज सिलवाने गया। और दर्जी से बोला-‘इस कमीज को नये फैशन में सिलना है। कमीज के दो बाजू, दो पल्ले और काॅलर तो होता ही है -‘बता तू नया क्या करेगा?’ दर्जी ने जवाब दिया-‘दादा! जहाँ चार छः बटन टाँकनेे हैं- मैं आठ टाँक दूँगा।’ दादा को अचानक एक आइडिया सूझा। उसने कहा- ‘भाई तू बटनों की संख्या बढ़ा!’ दर्जी ने फिर पूछा- ‘कितने बटन टाँकू ?’ दादा ने उसी रौ में कहा- ‘कहने को तो कमीज के दो पल्ले आपस में जुड़े होते हैं लेकिन- वे जुड़कर भी एक नहीं होते। दोनो पल्लों के बीच ‘छत्तीस का आँकड़ा’ होता है। इसलिए तू इस कमीज में छत्तीस बटन टाँक।’
तो बंधुओं यूं उन दादा की कमीज में छत्तीस बटन टँके। और वे जब तक जिंदा रहे- अपने मूल नाम से नहीं -‘छत्तीस बटन’ नाम से ही पहचाने जाते रहे और उसी नाम से दादागिरी करते चले गए।
सोच रहा हूं! आज अगर वे छत्तीस बटन वाले दादा होते -और प्रो. राजेश कुमार और डाॅ. लालित्य ललित की ये किताब ‘आँकड़ा तिरेसठ का’ का पढते तो दर्जी से सीधे बालतेे- ‘भाई इस कमीज में तिरेसठ बटन टाँक।’ कमीज में तिरेसठ बटन टाँकनेे के लिए भले ही जगह न होती -लेकिन दर्जी को टाँकनेे पड़ते। और दादा का हुलिया भले ही जो भी होता-तब लोग उन्हें ‘तिरेसठ बटन’ कहते। ऐसे ही मेरे इस शहर में फैशन के एक से एक स्टाइलिश नमूने निकलते रहे। उस समय फैशन के मामले में पेरिस पीछे था और पौड़ी आगे। लेकिन आज शहर के हालात आप देख ही रहे हैं।
दूसरी कहावत पौड़ी वासीयों के लिए ये प्रचलित थी कि किसी से भी सेखी बघारने के लिए या किसी के दवाब में आने से पूर्व -पौड़ी वासी कहता था-कि ‘इनै सूण! म्यरु घाट-घाटौ पाणी पीयूं! मैं सणी बेकूब नि समझी वा!’ (कम हियर! मैंने घाट-घाट का पानी पिया है, मुझे वेबकूफ मत समझना डियर!!)। थोड़ा मनन किया और मनन के बाद निष्कर्ष ये निकला कि ‘घाट-घाट का पानी पिया है’ कहने का आशय श्रीनगर के धोबी घाट और नान घाट से इस शहर में पहुंच रहे पानी से ही रहा होगा।
लेकिन अब इस शहर के वे सब बम्बू उखड़ चुके। कनाथ-परदे सब बदल गए हैं। और धरातल पर – कुत्ते, कूड़ा, कचरा, सुअर, बन्दर, किरायेदार और हम जैसे कुछ किरदार रह गए हैं। जो न इधर के हैं-न उधर के हैं।
सबसे पहले किरायेदारों से क्षमा निवेदित है। आप कुत्ते, कूड़ा, कचरा, सुअर, बन्दर और हम जैसे नमूनों के साथ अपने उल्लेख को अन्यथा न लें।
किरायेदार बंधुओं…! किरायेदार होना कोई बुरी बात नहीं है- हमारी मजबूरी है। वर्ना कौन नहीं चाहता -शहर में उसका भी मकान हो। मकान के नीचे दुकान हो। लेकिन जरूरी नहीं कि हर किसी के भाग्य में मकान और दुकान दोनो हो। जहां तक किरायेदार की बात है तो इस शहर में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, भारत सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री अग्रज श्री निशंक जी भी किरायेदार रह चुके हैं। एक समय तो ऐसा भी था जब उन्होंने तंगहाली में भी दो-दो जगह का किराया चुकता किया। एक जगह चारपाई का दूसरी जगह प्रेस का।
इस शहर में वे नौनिहाल जो पढ़ रहे हैं- और किराया दे रहे हैं। मन लगाकर पढ़ते रहें। किरायेदार अगर बात-बात पर खिच-खिचकर करे-तो अपने कानों पर रूईं डाल दें। और अगर वो किराया देने पर भी बार-बार कमरे में घुसकर अपनी धौंस दिखाए-तो झगरा मोल न लें। कमरा बदल दें। भई! ऐसी मुसीबतें तो तुलसी दास जी भी- काशी में बहुत झेले हैं। प्रो. काशीनाथ सिंह ने अपनी पुस्तक ‘काशी का अस्सी‘ में ‘सन्तों झगरा में झगरा भारी’ अध्याय में लिखा है- ‘तुलसी बाबा अस्सी घाट पर आए और डेरा-डंडा जमाया। बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी उन्हें,कभी लंगोटी गायब होती, कभी धोंकरा, कभी लुटिया,कभी कंमडल, कभी पोथी। वे भागते फिरे यहां से वहां-कभी गोपाल मन्दिर, कभी हनुमान, फाटक,कभी राजा दरवाजा,कभी बिन्धुमाधव मन्दिर, बड़ा दिक किया मुहल्ले ने।’ लेकिन तुलसी बाबा ने न अस्सी छोड़ा न काशी।
मेरे नौनिहाल किरायेदारों…! आपके पास भी पौड़ी गांव में न सही पास में च्वींचा-कांडई-बैंज्वाड़ी गांव हैं। सर्किट हाऊस मोहल्ला, क्यूंकालेश्वर मोहल्ला, पितृ मोहल्ला, थाना मोहल्ला, न्यू विकास कालोनी, विकास मार्ग, लक्ष्मीनारायण से लेकर बुबाखाल और श्रीनगर मार्ग पर पे्रमनगर तक आपके विकल्पों की कमी नहीं। तुलसी बाबा का ध्यान करें -शहर कदापि न छोड़ें। मेरे भी तीन घनिष्ठ मित्र मेरे किरायेदार रहे हैं। और जब तक रहे अकड़ कर रहे।
बंधुओं! इस शहर में किरायेदारी की बहुत पुरानी परम्परा है। इस शहर में न सही कहीं और किरायेदार रहा हूं। इसलिए किरायेदारों की दिक्कतें जानता हूं। इसी शहर के निचले हिस्से में किराये पर रहने वाले नेपाली मजदूरों की दिक्कतों के किस्से भी मैंने खूब सुने हैं। दस बाई दस की खोली में भी वे दस-दस रहते थे। कुछ लोग कहते हैं वे कमरे नहीं मकबरे थे। लेकिन उन्हें कमरे कहें या मकबरे -उनमें वे मजदूर बेचारे दिन ही नहीं रात में भी बड़े तकलीफ में रहते थे। सोते हुए मनमाफिक करवट भी नहीं बदल सकते थे। एक ही करवट में सोते -सोते जब किसी की बांह दुखने लगे -या कोई करवट बदलना चाहे -तो वे करवट भी नहीं बदल सकते थे। इस मुसीबत से निबटने के लिए उन्होेंने एक तरकीब अपनानी शुरू की। कह नहीं सकते वो उनमें से किस नेपाली के दिमाग की उपज थी। लेकिन सुना है बड़ी कारगर साबित हुई। उनमें से एक ही करवट लेटे लेटे जिसकी बांह पहले दुखती-उसको तीन अक्षर के एक शब्द कहने की अनुमति दे दी गई थी। वह शब्द था- ‘फरको!’ याने की ‘पलटो’ अर्थात ‘सब एक साथ पलटो!’ बंधुओं! इस शहर के विकास को उलटने-पलटने वालों ने नहीं ऐसे ही मेहनत कश लोगों ने गति दी।
अगर कोई ये सवाल पूछे कि- ‘इस शहर में सबसे ज्यादा दुर्गति किसकी हुई? तो एक ही जवाब है- कुत्तों की! उनको अलग चारपाई, अलग गद्दा, अलग थाली,अलग चम्मच की आदत किसने डाली? सुबह-साम मालिक के साथ घूमगस्ती। लेकिन आप हैं कि ही शहर ही छोड़कर चले गए। कुत्ते घर के रहे न घाट के । बेचारे सड़क पर आ गए। दुनिया का क्या? उन्हीं के सामने कह देते है-‘ये आवारा कुत्ते हैं!’ लेकिन कोई उन्हें एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं देते हैं। सत्य कहें कुत्तों की ऐसी विकट परिस्थिति में हर भर के ‘बूचड़ खाने’ ही उनके अनाथालय हैं।
लेकिन शहर के सुअरों की भी बड़ी कुदशा है। आदमी उनसे चिढ़ते हैं और कुत्ते उनपर भौंकते हैं। जबकि शहर भर में सूअर ही एक ऐसे हैं जो पूर्णतः आत्मनिर्भर है।
एक और है इस शहर के अन्दर। वो है- बन्दर! ये बन्दर बाल बच्चों के संग हैं। संगठित हैं लेकिन मर्यादा विहीन नंग धड़ंग हैं। कुत्तों, सुअरों के बाद ये शहर में हालिया घुसपैठिए हैं। मौका मिलते ही जहां चाहे धावा बोल देते हैं। बाॅउन्ड्री के अन्दर आने के बाद बन्दर कभी ये नहीं पूछते- ‘अरे भाई कोई घर में है?’ या- ‘है कोई इस घर के अन्दर?’ वे पास पड़ोस में किसी से पूछताछ करके भी नहीं आते। कि फलां व्यक्ति के घर पर कोई है या नहीं है? वे केवल ये देखते हैं कि आस-पास जो बैठे हैं -वे ऊंघ रहे हैं- या जाग रहे हैं। और जब तसल्ली हो जाती है तो इतमिनान से अन्दर घुस जाते हैं। जो कुछ उन्हें मिल जाय -खाते हैं। जितना हो सके उत्पात मचाते हैं। और कभी-कभी आटे का थैला खाली कर ‘आटा स्नान’ कर चुपके से बाहर निकल जाते हैं।
शहर के कुत्ते, कूड़ा, कचरा, सुअर, बन्दर और किरायेदार के बाद-हम हैं जो कुछेक हैं। आप फिर पूछोगे- ‘हम कुछेक कौन है?’ ऊपर लिखा तो है – ‘नमूने हैं!’ आप आगे पूछोगे-‘हम नमूने कैसे हुए?’ अरे हुए तो वैसे ही जैसे ‘विकास’ हुए। लेकिन हमारी बात कुछ है। जैसे लोग कहते हैं मैं मौन हूं। वैसे ही सब मौन हैं। दरअसल ये मौन ही हमारी साधना है। अगर हमें न्याय संगत तराजू पर तोलें-तो एक पले एक पलड़े में हमारा मौन मिलेगा दूसरे पलड़ में हमारी साधना। लेकिन साधना में हैं तो क्या हम घंटा-शंख न बजाएं। लेकिन आप ये आरोप लगाते हैं कि – जहां हाथ उठाने की जरूरत होती है वहां हम सावधान मुद्रा में आ जाते हैं- और जहां टांग रखने की जगह नहीं होती-वहां टांग अड़ा देते हैं।
एक ने पूछा -‘ये किसने कहा?’
मैंने जवाब दिया-‘विकास’ ने!
-‘अरे वो ‘विकास’ जो कई दफा फेल हुआ- और आप उससे डर गए! ’
मैंने कहा-‘डरा नहीं खड़ा रहा। और मैं मरते दम तक खड़ा रहूंगा! मालूम है पिछली रात मैंने सपने में क्या देखा?’
-क्या देखा?
-मेरे आस-पास शहर भर के लोग जमा हैं। कुछ लोग कह रहे हैं- मुझपर राजनीति का भूत सवार है। वे चिंता में हैं कि मेरा ये राजनीति का भूत कैसे उतरे? कुछ लोग कह रहे हैं – इसको उठना चाहिए। और कुछ लोग कह रहे हैं -नहीं इसको नहीं उठना चाहिए! लेकिन किस्सा कुर्सी का था। मैं जानता हूं मुझमें उठने की क्षमता नहीं है- लेकिन मैं उठा! सपने में ही देख रहा कि इस बार का चुनाव भी कूड़े कचरे के मुद्दे पर ही लड़ा जा रहा। मैं भावावेश में प्रतिद्वंदी को सरेआम ‘कचरा’ बोल गया। फिर प्रतिद्वंदी ने भी भरी जनसभा में मुझे ‘कूड़ा’ कहा। जब तक चुनाव नहीं निबटा तब तक शहर भर में ‘कूड़ा’ और ‘कचरा’ ही छाया रहा। शहर ही नहीं पूरे जनपद में ‘कूड़े’ और ‘कचरे’ की ही चर्चाएं होती रही।
लोगों में एक ही चिंता आम थी कि- इस छोटे से शहर का ये हाल है तो प्रदेश और देश के कूड़े और कचरे की स्थिति तो और भी भयानक होगी। पहाड़ में तो पब्लिक कम है लेकिन बड़े शहर और महानगरों में लोगों को नींद कैसे आती होगी?
धुंवाधार प्रचार होता रहा। सड़कों, चौराहों और चौपालों को बैनरों पोस्टरों से पाट दिया गया। आम सभाओं में मुझे ‘कूड़ा जिंदाबाद’ और मेरे प्रतिद्वंदी को ‘कचरा मुर्दाबाद’ सुनाई देता रहा। प्रचार थमा। बोटिंग हुई। फिर गिनती हुई। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। सबने कहा- ‘जीत गया-हमारा भाई जीत गया!’ पत्नी ने पूछा- ‘कौन जीता?’ मैंने जवाब दिया- ‘आपका कूड़ा!’
बंधुओं! ये भी मैंने सपने में ही देखा- सालों बाद भी मेरे घर पर कूड़ा, सर पर कूड़ा, शहर भर में जहां देखो कूड़ा ही कूड़ा बिखरा पड़ा।
एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा- ‘भाई ये कूड़ा कब उठेगा?’
दूसरे ने जवाब दिया -‘जब हाई कमान चाहेगा!’
मैंने कहा- ‘करतूत तुम्हारी मैं क्यों अपने सर पर लूंगा? मैं लड़ूंगा! मैं जरूर लड़ूगा! और अन्तिम सांस तक इस कूड़े, इस कचरे के खिलाफ लडूंगा!!’
‘विकास’ यात्रा जारी है…..
(चित्र साभार सोशल मीडिया से!)