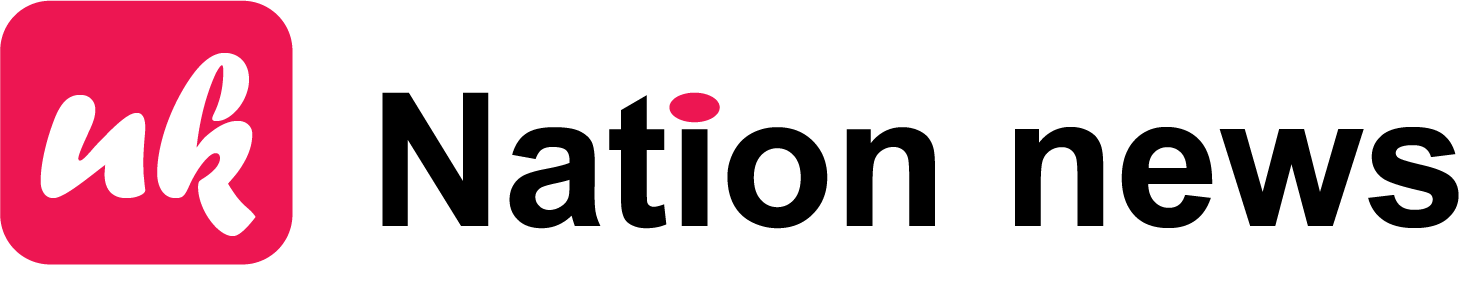भारतीय न्यायपालिका, विश्वास का ह्रास ?


प्रो. नीलम महाजन सिंह
भारतीय न्यायपालिका, जिसे अक्सर भारतीय संविधान का संरक्षक व न्याय का रक्षक कहा जाता है, भ्रष्टाचार के अभिशाप से अछूती नहीं है। न्यायपालिका, जिसे न्याय चाहने वाले आम आदमी के लिए उम्मीद का आखिरी गढ़ माना जाता है, भ्रष्टाचार व भाई-भतीजावाद के आरोपों से घिरी हुई है। यह मुद्दा भारत के नागरिकों के लिए चिंता का विषय रहा है व इसने न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता और अखंडता पर प्रश्न खड़े किए हैं। इस लेख का उद्देश्य पाठकों के सामने यह प्रस्तुत करना है कि न्यायिक कार्यों में भ्रष्टाचार कैसे होता है, ऐसे कौन से उदाहरण हैं जिनमें न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं व संस्था में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूर्ण न्यायपालिका ही अविश्वसनीय है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कैसे होता है? भारतीय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार कई रूपों में होता है, जिसमें रिश्वतखोरी व पक्षपात से लेकर भाई-भतीजावाद व राजनीतिक हस्तक्षेप तक शामिल हैं। न्यायाधीशों को कथित तौर पर अनुकूल निर्णय देने के लिए रिश्वत दी जाने के आरोप लगाए गए हैं। इससे न्याय की नींव कमज़ोर हुई है और न्यायपालिका में जनता का भरोसा कम हुआ है। जजों पर कथित तौर से व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर कुछ व्यक्तियों या पार्टियों के प्रति पक्षपात दिखाया गया है। भ्रष्टाचार का एक और रूप मामलों के आवंटन या बेंचों के गठन के दौरान होता है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जब हमारी प्रतिष्ठित न्यायिक संस्था भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए जांच के दायरे में आई है। उदाहरण के लिए, 2017 में, न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन, जो मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन्हें न्यायालय की अवमानना के लिए छह महीने के कारावास की सज़ा सुनाई गई जो उनहोंने पूरी कर ली है। 2019 में सीबीआई ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नारायण शुक्ला पर अवैध रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप और तेलंगाना में निचली अदालतों के तीन न्यायाधीशों को आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए सज़ा सुनाए जाने जैसे अन्य उदाहरण हैं, जिनमें न्यायपालिका में जनता का विश्वास डगमगाया है। न्यायपालिका में बढ़ते भ्रष्टाचार के लिए अनेक कारक हैं। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक पारदर्शिता व जवाबदेही की कमी है। न्यायिक नियुक्तियों और पदोन्नति की अपारदर्शी प्रकृति ने अक्सर पक्षपात व भाई-भतीजावाद के आरोपों को जन्म दिया है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, राजनीतिक हस्तक्षेप और योग्यता-आधारित चयन की कमी के आरोप के विवाद का विषय हैं। इसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता व निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं।न्यायपालिका में भ्रष्टाचार में योगदान देने वाला एक अन्य कारक मामलों का अत्यधिक लंबित होना है। न्याय वितरण की धीमी गति ने ऐसा माहौल बनाया है जहाँ वादी अपने मामलों को तेज़ी से निपटाने के लिए वैकल्पिक साधनों की तलाश करने के लिए मज़बूर हैं। इसने भ्रष्टाचार के अवसर पैदा किए हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने मामलों को तेज़ी से निपटाने के लिए अदालत के अधिकारियों या न्यायाधीशों को रिश्वत देने का सहारा ले सकते हैं। न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए मौजूदा तंत्र, जैसे कि महाभियोग प्रक्रिया, बोझिल व अक्सर अप्रभावी है। इसने दंड से मुक्ति की संस्कृति को जन्म दिया है, जहां न्यायाधीश अपने कार्यों के लिए जवाबदेही से अलग-थलग महसूस करते हैं। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पूरी तरह से असहिष्णु क्यों है? न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का प्रभाव दूरगामी है। यह न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को खत्म करता है व कानून के शासन को कमज़ोर करता है। यह दंड से मुक्ति की संस्कृति को भी कायम रखता है, जहां सत्ता व प्रभाव वाले व्यक्ति अपने फायदे के लिए सिस्टम में हेरफेर कर सकते हैं। इसके अलावा, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का आम नागरिकों के जीवन पर सीधा असर पड़ता है, जिन्हें समय पर निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाता। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की ज़रूरत है। सबसे महत्वपूर्ण, न्यायिक नियुक्तियों व पदोन्नति में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की ज़रूरत है। योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया, कड़े नैतिक मानकों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है कि केवल सबसे योग्य व निष्पक्ष व्यक्ति ही न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाएं। कोलिजियम (collegium) सिस्टम पर अनेक प्रश्नचिन्ह हैं। न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों को दूर करने के लिए एक मज़बूत तंत्र की ज़ररत है। न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार व कदाचार के आरोपों की जांच के लिए जांच शक्तियों के साथ एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। इससे जनता में विश्वसत करने में मदद मिलेगी, कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यहां तक कि वे भी नहीं जिन्हें कानून को बनाए रखने का काम सौंपा गया है। केस प्रबंधन में सुधार और मामलों के समाधान में तेज़ी लाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से भी इस मुद्दे को हल करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों पर अधिक से अधिक जन जागरूकता व सहभागिता की आवश्यकता है। नागरिक समाज संगठनों, मीडिया व नागरिकों को न्यायपालिका को जवाबदेह बनाने और इसके कामकाज में पारदर्शिता की मांग करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। न्यायालय की फाइलों व अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, ई-कोर्ट कार्यवाही का संरक्षण, प्रौद्योगिकी का कुशल उपयोग प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ाएगा। निष्कर्ष में, भारतीय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एक गहरा मुद्दा है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। कानून के शासन को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय सभी के लिए सुलभ हो, इस मुद्दे को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने व न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए न्यायपालिका, सरकार, नागरिकों, समाज और सभी हितधारकों के एक साथ प्रयास की आवश्यकता है। तभी न्यायपालिका भारत में न्याय के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को सही मायने में पूरा कर सकती है। अक्सर, संस्था में भ्रष्टाचार के अभिशाप के संबंध में न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणियां की जाती हैं। इसलिए, न्यायपालिका के इच्छुक लोगों के लिए न केवल प्रणाली में भ्रष्टाचार के बारे में बल्कि इसे खत्म करने के तरीकों और प्रणाली में सुधार और जवाबदेही लाने के बेहतर तरीकों के बारे में भी जागरूक होना आवश्यक है। जहां सत्यमेव जयते, हमारे संविधान का प्रतीक है, वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जस्टिस तीर्थ सिंह ठाकुर, जस्टिस एस. मुरलीधर, जस्टिस दीपक गुप्ता, व 21 हस्ताक्षरकर्ताओं में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दीपक वर्मा, कृष्ण मुरारी, दिनेश माहेश्वरी व एम.आर. शाह तथा हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश प्रमोद कोहली, एस.एम. सोनी, अंबादास जोशी और एस.एन. ढींगरा शामिल हैं। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में न्यायपालिका को ऐसे दबावों से खुद को बचाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी कानूनी प्रणाली की पवित्रता व स्वायत्तता बनी रहे। यह ज़रूरी है कि न्यायपालिका लोकतंत्र का स्तंभ बनी रहे व स्थायी राजनीतिक हितों की सनक से मुक्त रहे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश जस्टिस मदन लोकूर तथा वरिष्ठ अधिवक्ताओं में, दुष्यंत दवे, रविंद्र गुप्ता, सलमान खुर्शीद तथा अनेक न्यायविदों ने संविधान की सुरक्षा के लिए पारदर्शिता व सत्यता का आह्वान किया है।

प्रो. नीलम महाजन सिंह
(वरिष्ठ पत्रकार, राजनैतिक विश्लेषक, शिक्षाविद, दूरदर्शन व्यक्तित्व व सालिसिटर फाॅर ह्यूमन राइट्स)
singhnofficial@gmail.com
(THE VIEWS EXPRESSED IN THIS ARTICLE SRE PERSONAL VIEWS OF THE WRITER )