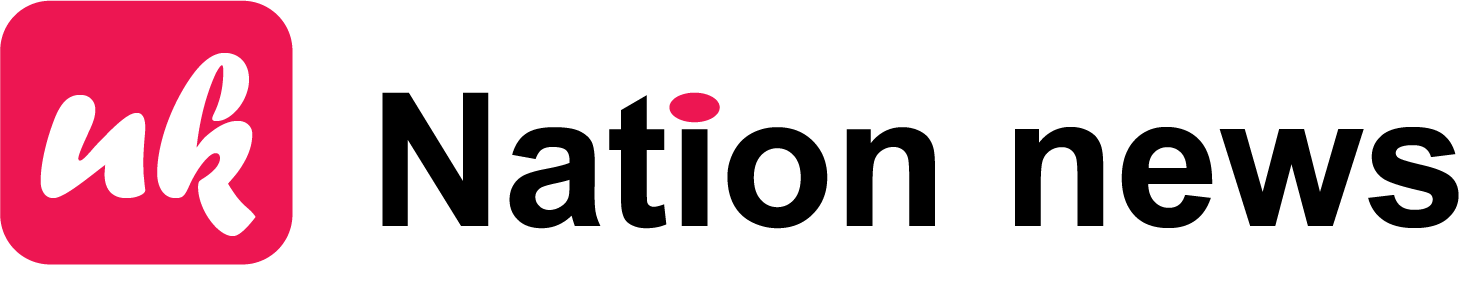पर्वतीय लोककला मंच और जोधा फिल्म्स ने की दिल्ली में एक खुली परिचर्चा जिसका विषय था- ‘उत्तराखंड रंगमंच एवं फिल्म: दशा और दिशा।’

VYOMESH JUGRAN
पर्वतीय लोककला मंच और जोधा फिल्म्स ने हाल में नई दिल्ली में एक खुली परिचर्चा की जिसका विषय था- ‘उत्तराखंड रंगमंच एवं फिल्म: दशा और दिशा।’ इसमें लेखन व कला जगत की विभिन्न विधाओं के कई मूर्धन्य हस्ताक्षरों ने हिस्सा लिया।
परिचर्चा में उत्तराखंड के जानेमाने फिल्म प्रोड्यूसरों, नाटककारों और कलाकारों का यह एकालाप रोचक था कि उत्तराखंडी सिनेमा और रंगमंच, दोनों विधाओं की दशा खराब चल रही है और दिशा का भी पता नहीं है। खासकर प्रोड्यूसर संजय जोशी, निर्देशक अनुज जोशी, नाटककार हरि सेमवाल और लक्ष्मी रावत के बयान ऐसे थे, मानो वे फिल्मकार/नाटककार न होकर दर्शकों की पांत में बैठ गुणवत्ता पर गरियाने वाले आलोचक अथवा समीक्षक हों। सुश्री लक्ष्मी रावत यदि पर्वतीय रंगमंच और सिनेमा के अतीत को याद कर कहती हैं- दौर अच्छा था, है नहीं… तो माफी के साथ कहना चाहेंगे कि हाल में मंचित अपने नाटक ‘ल्यावा बणिगे हमरि बि फिलम’ में वह चाहकर भी यह संदेश देने का साहस क्यों नहीं जुटा सकीं कि उत्तराखंडी फिल्में ‘मसालेबाजी’ से ऊपर नहीं उठ पा रही हैं!
इस खुली परिचर्चा का कुशल संचालन पर्वतीय लोककला मंच, नई दिल्ली के महासचिव हेम पंत ने किया। मंच पर अकादमी पुरस्कार से सम्मानित समीक्षक दीवान सिह बजेली, साहित्यकार डॉ. हरिसुमन बिष्ट, उद्यमी नरेन्द्र सिंह लडवाल, अणुव्रत सेवी व चिन्तक रमेश काण्डपाल, रेलवे उपक्रम में प्रबंध निदेशक एचबी जोशी, जेडीएस ग्रुप के एमडी संजय जोशी, राजनीतिक व्यक्तित्व पीसी नैलवाल और पर्वतीय लोक कला मंच के अध्यक्ष हीरा बल्लभ काण्डपाल विराजमान थे।
सर्वश्री मनोज चंदोला, राकेश गौड़, भूपेश जोशी, डॉ. कमल कर्नाटक, सुशीला रावत, दिनेश फुलारा, चन्द्रमोहन पपनै, रमेश घिल्डियाल और चारू तिवारी जैसे प्रबुद्धों ने भी अपने विचार रखे। जानेमाने रंगकर्मी डॉ. सतीश कालेश्वरी, रमेश ठंगरियाल, महेन्द्र लटवाल, अजय बिष्ट, हरेन्द्र रावत, खुशहाल बिष्ट, उमेश बंदूनी, ममता कर्नाटक, कुसुम चौहान, भुवन सिह, खुशहाल सिंह रावत और वरिष्ठ पत्रकार सुनील नेगी इत्यादि की उपस्थिति ने भी खुली चर्चा को गरिमा प्रदान की।
मुख्य बात यह उभर कर आई कि कैमरा, तकनीक, गायिकी, संगीत, अभिनय और संबंधित विधाओं में पारंगत कलाकारों की वरदानी शक्ति के बावजूद उत्तराखंडी फिल्में और नाटक पहले जैसा सम्मोहन क्यों नहीं पैदा कर पा रहे! सुझाव दिए गए कि आंचलिक नाटक भारतीय परंपरा में हों, गैर-उत्तराखंडी दर्शकों को भी लक्षित किया जाए, रंगमंच और सिनेमा एक-दूसरे का पल्लू थामकर चलें, नई पीढ़ी को जोड़ें, मिलजुल कर काम करें, प्रोडक्शन का प्रमुख उद्देश्य कला हो, अपनी समृद्ध परंपरा और संस्कृति का राग न अलापते रहें, रिहर्सल पर अधिकाधिक जोर दें, कलाकारों को मेहनताना मिले, कम बजट में लोकजीवन पर आधारित अच्छी फिल्में बनें, सब्सिडी को थियेटर निर्माण इत्यादि पर खर्च किया जाए और डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रयोगवादी सोच का निर्माण हो इत्यादि।
पहली गढ़वाली फिल्म ‘जग्वाल’ 1983 और कुमाऊंनी ‘मेघा आ’ 1987 में आई थी। सालों तक सबकुछ ठहरा रहा, पर अब फिल्मों की बाढ़ सी आ गई है। ऐसे में ‘दशा और दिशा’ जैसी खुली परिचर्चाएं स्वागत योग्य हैं। पर्वतीय सिनेमा के लिए कंटेंट की कमी नहीं है। कुछ लोगों ने शानदार काम किया भी है। लेकिन चूंकि आंचलिक सिनेमा का दर्शक वर्ग सीमित होता है और ज्यादातर मामलों में फिल्मकार की ख्वाहिश होती है कि वह अधिकाधिक दर्शकों तक पहुंचे। लिहाजा वह ऐसे कथानक चुनने की ताक में रहता है जिसे हिन्दी व अन्य भाषाओं में भी डब किया जा सके। उसका यही मोह सार्थक सिनेमा और मसालेदार सिनेमा के अंतर को मिटा डालता है। तब ज्यादातर पहाड़ी फिल्में प्रेम के सामान्य कथानक और फार्मूलेबाजी से ऊपर नहीं उठ पातीं।
संबंधित परिवेश को आत्मसात करती अभिव्यक्ति का न होना भी पर्वतीय फिल्मों की एक बड़ी कमजोरी है। कथावस्तु यदि गांव की चारित्रिक विशेषताओं से मेल नहीं खाएगी तो अभिनय कर रहे पात्र गांव का हिस्सा नहीं लगेंगे। कितने कलाकार या निर्देशक हैं जो फिल्म निर्माण से पहले गांव के रोजमर्रा के वातावरण को आत्मसात करने की जहमत उठाते हों! प्रख्यात लोकगायक नरेन्द्र सिंह नेगी की सीख सामने है। पौड़ी गांव के वातायन को आत्मसात कर ही वह कालजयी गीतों की रचना कर सके। वह स्वीकार करते हैं कि पर्वतीय महिला के अनकहे दर्द को स्वर देते उनके गीतों के पीछे गांव का श्रमसाध्य जीवन है जिसकी नायिका उनकी मां खुद हैं।
उत्तराखंडी फिल्मों के चरित्र अभिनेता या साइड कलाकार तो संवाद अदायगी में माहिर हैं, मगर नायक-नायिका ठेठ गढ़वाली ‘ढौळ’ नहीं निकाल पाते। यहां चयन में सुंदरता ही एकमात्र पैमाना क्यों हो! बोली-भाषा और अभिनय में सिद्धहस्त आम चेहरे नायक-नायिका क्यों नहीं हो सकते! जहां तक कहानी की बात है, पहाड़ में लोकजीवन से जुड़ी एक से बढ़कर एक कथाएं/ घटनाएं मौजूद हैं। पर, उनसे इतर अजीबोगरीब कहानियों को लेकर फिल्में बन रही हैं। बात हॉरर मूवी तक पहुंच चुकी है।
ऐसी लोकचेतना जिसमें पहाड़ के बुनियादी सरोकारों को संबोधित किया जा रहा हो, कम नजर आती है। लोकचेतना का यह लोप उत्सवी वातावरण में डूबे पर्वतीय समाज के बावजूद है। गढ़वाली-कुमाउंनी कवियों का एक बहुत बड़ा वर्ग उपजा है, दर्जनों किताबें छप रही हैं और धामिर्क अनुष्ठानों-आयोजनों से अखबार और सोशल मीडिया पटा पड़ा है। क्या इसका कोई सकारात्मक प्रभाव समाज पर है या यह स्थिति एक ‘सांस्कृतिक अतिवाद’ की द्योतक है। कम से कम सरकारों को तो यह सब खूब रास आ रहा है। उनके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति यही है कि ‘समस्याओं का पहाड़’ सांस्कृतिक अतिवाद के साए में अलसाता रहे। यही वह मोड़ है, जहां से एक सरोकारी रंगमंच और सिनेमा धारदार उत्तर दे सकता है।