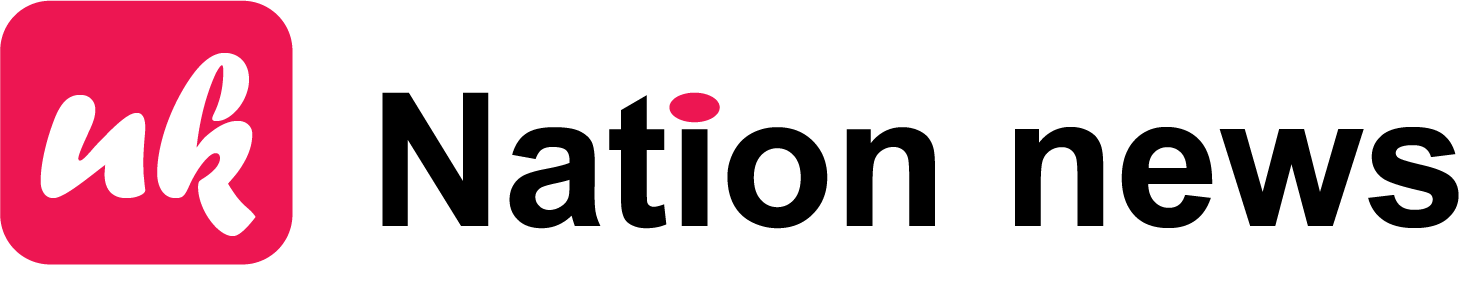गढ़वाली को बोली, उपबोलियों के संकीर्ण दायरे से मुक्त करें!
गढ़वाली भाषा है! सचेतन सगर्व कहें!

नरेन्द्र कठैत
पगडंडी से साथ-साथ उतरते 10-12 वर्ष की वय के बालकों से मुखातिब हो पूछा- ‘आपको गढ़वाली आती है?’ दोनों ने साथ-साथ सगर्व जवाब दिया-‘जी!’ आगे पूछा- ‘क्या है गढ़वाली! बोली, दूदबोली, मातृभाषा, लोकभाषा या भाषा?
’ एक ने कहा- ‘अंकल जी! गढ़वाली बोली है!’ प्रति प्रश्न किया -क्यों? उत्तर मिला -‘क्योंकि यह हमारे यहां बोली जाती है।’ और अंकल जी इसको हम ‘दूदबोली’ भी कहते हैं !
ठीक! इसी सवाल पर दूसरे का सपाट उत्तर था – ‘अंकल जी! गढ़वाली भाषा है! और यह हमें हमारी माता से संस्कारों में मिली है इसलिए इसे ‘मातृभाषा’ भी कहते हैं। अंकल जी! सारे क्षेत्र के लोगों द्वारा कही जाती है इसलिए यह हमारी ‘लोक भाषा’ भी है।’
आगे पूछा- गढ़वाली पढ़ते हो?
-हां कभी -कभी!
-सुनते हैं?
- रोज जी! किसी न किसी को लाइव हर दिन हर घड़ी!
-भाषा से सम्बन्धित जो बात ज्यादा सुनी?
-आठवीं अनुसूची!
बड़े प्लेटफार्म पर भी मूलतः गढ़वाली की यही स्थिति है जी! गढ़वाली आती है?-जी! सुनते हैं?- रोज जी! किसी न किसी को लाइव हर दिन हर घड़ी! पढ़ते हैं?-कभी-कभी। और भाषा से सम्बन्धित रटी रटाई एक ही चीज- आठवीं अनुसूची! इतना होने पर भी एक आश्चर्य और है जी! आज भी गढ़वाली ‘लोकभाषा’ और ‘भाषा’ दो खेमों में है बंटी हुई। ऐसी विकट स्थिति में आवश्यकता समाधान की है न कि तटस्थता की। हालांकि लोकभाषा और भाषा के द्वंद में भाषा निर्द्वन्द है जी! किंतु सबसे पहले यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि ‘बोली’ अथवा ‘भाषा’ आखिर है क्या चीज?
‘भाषा तत्व और आर्य भाषा का विकास’ में शिवराज सिंह रावत ‘निःसंग’ लिखते हैं- ‘जन समाज में प्रचलित शब्दावली और उसे बरतने के ढंग को बोली या भाषा कहा जाता है। बोली या बोलियों के संस्कारित स्वरूप को यदि भाषा कहा जाय तो इसमें कोई उत्युक्ति नहीं होगी। ….आकाश में तैरने वाली वाणी जब सार्थक ध्वनि या शब्द मंत्र द्रष्टा ऋषियों को ध्यान में सुनाई दी तो वह बोलकर भावप्रकाश करने का साधन बन गया। जिसे आज भाषा कहा जाता है। इस प्रकार भाषा एक शब्द योजना है। स्पष्ट है कि ध्वनियों से शब्द, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा बनती है। अपने प्रारम्भिक काल में कोई भी भाषा बोली ही होती है। अर्थात् भाषा की उत्पत्ति बोली से होती है।’
उत्तराखण्ड के परिवेश से बाहर से समझने का प्रयत्न करें तो ‘साहित्य और संस्कृति’ में अमृत लाल नागर उदृत करते हैं- ‘जबान या भाषा कोई बनाता नहीं है, वह तो जन-टकसाल ही में ढ़लती है। कुदरती हालात उसे बनाते हैं। कवि, कलाकार, साहित्यिक उसे संवारते हैं और शिष्ट समाज उसकी मर्यादा बढ़ाता है।’
शिवराज सिंह रावत ‘निःसंग’ तथा अमृत लाल नागर जी ने उपरोक्त उद्धरणों में दो शब्द युग्म प्रयुक्त किये हैं- ‘जन समाज’ और ‘जन टकसाल‘- अर्थात जन की भाषा या लोकभाषा!
यह प्रश्न अक्सर सर उठाता है -‘ गढ़वाली भाषा है अथवा लोकभाषा?’ हालांकि अपनी पुस्तक ‘गढ़वाली भाषा की शब्द-संपदा’ में भाषाविद अग्रज रमाकान्त बेंजवाल ने गढ़वाली के लोक भाषा और भाषा दोनों पक्षों के मूलभूत तत्वों को विस्तार से रखा है। लेकिन फिर भी यह स्पष्ट लिखा है कि-
‘गढ़वाल क्षेत्र में बोली एवं लिखी जाने वाली भाषा गढ़वाली कहलाती है।’
भाषा के इंही स्वरूपों के इर्द-गिर्द एक अन्य शब्द है- ‘मातृभाषा!’ दरअसल हम कई भाषाओं के ज्ञाता हो सकते हैं लेकिन मातृभाषा हमारी एक ही होती है। अन्य भाषाओं के मुकाबले मातृभाषा में हमारी संप्रेषण शक्ति अधिक होती है।
‘अक्षर पर्व’ के नवम्बर 1999 के अंक में इसी क्षेत्र के मूल से जुड़े कलमकार श्री मंगलेश डबराल लिखते हैं -‘ इस देश में किसी की भी भाषा हिन्दी नहीं है। आपकी छतीसगढ़ी होगी या बुंदेलखंडी होगी, भोजपुरी होगी। मेरी जो भाषा है वो गढ़वाली है। लेकिन में हिंदी में लिखता हूं। हिंदी की कविता लिख रहा हूं। जबकि वाचिक परम्परा लोक स्मृति में ही आ सकती हैं उसके लिए मुझे लगता है कि एक भाषा का लोकभाषा होना जरूरी होगा तभी वाचिक परम्परा बची रहेगी। हिन्दी के साथ संकट है वह किसी की भी भाषा नहीं है। वाचिक परम्परा का नष्ट होना इसी का परिणाम है।’ अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक ‘गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य’ में डाॅ हरिदत्त भट्ट ‘शैलेश’ ने भी स्पष्ट लिखा है कि ‘गढ़वाली मेरी मातृभाषा है।’
अर्थात भाषा का मूल लोक भाषा है। किंतु लोक से पहले वह हमारी मातृभाषा है। हमारी माता इसकी पहली पाठशाला है। किंतु यह तथ्य भी है सर्वसत्य है कि मातृभाषा सीखने की कोई उमर नहीं होती। दार्शनिक श्री अरविन्द आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं। कहीं उल्लेख मिला है कि किशोर अरविन्द को भारत में रहते हुए कभी अपनी मातृभाषा बंगला सीखने का अवसर नहीं मिला। उन्हें या तो अंग्रेजी आती थी या हिंदी। इंग्लैंड में टावर्स नामक अंग्रेज से बंगला सीखनी शुरू की।
आचार्य विनोबा कहते हैं -‘बाल्यावस्था में बालक जिस सहज भाव से मातृभाषा सीखता हैं उसी सहज भाव से उसका अगला शिक्षण भी होना चाहिए। लड़का, व्याकरण क्या चीज है,यह भले ही न जानता हो, लेकिन वह मां आया नहीं कहता। कारण वह व्याकरण समझता है। वह व्याकरण शब्द भले ही न जानता हो या उसे व्याकरण की परिभाषा भले ही न मालूम हो, परन्तु व्याकरण का मुख्य कार्य तो हो चुका है।’ माता कभी भी मातृभाषा का गलत उच्चारण नहीं करती। खाते को खाती, पीते को पीती और जाते को जाती नहीं कहती। क्या यह सही नहीं कि अनपढ़ होने पर भी उसे ‘व्याकरण’ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती।
‘भाषा तत्व और आर्य भाषा का विकास’ में शिवराज सिंह रावत ‘निःसंग’ मातृभाषा को प्राकृत रूप को और गहराई से जोड़कर कुछ यूं देखते हैं- ‘मानुष की प्राकृत भाषा के शिक्षकों में सबसे ऊंचा स्थान ‘कौआ’ का है। वह कई प्रकार की बोली बोलता है। बोली बोलते समय वह अपनी पूंछ को नीचे झुकाता है। विविध प्रकार के शब्द निकालने के लिये वह अपनी चोंच को कई बार दायें-बायें ऊपर नीचे करता है। प्राकृत का अर्थ है स्वाभाविक।’
मनुष्य की प्राकृत भाषा के शिक्षकों के स्रोत के रूप में कौवे को जोड़े या मां के सर्वोच्च स्थान से आगे बढ़ें। मुख्यतः भाषा का यह स्वरूप वाचिक परम्परा का ही द्योतक हैं। मंगलेश जी ने वाचिक परम्परा के हरास के जिस संकट को हिंदी भाषा के सामने महसूस किया है गढ़वाली भाषा भी उससे अछूती नहीं है। गढ़वाली भाषा की मौलिक वाचिक परम्परा आज भी गांवों तक ही सीमित है। गढ़वाली भाषा का शहरी परिवेश मूल से भिन्न अन्य से ट्रांसप्लान्टैड है। इसीलिए वर्तमान में अधिकांश लेखन न केवल हमारी समझ से बाहर बल्कि मूल भाषा के लिए भी घातक है।
भाषा की यह भिन्नता कैसे? इस संबंध में ‘गेहूं और गुलाब में श्री रामवृक्ष बेनीपुरी’ के लिखे ये शब्द भी विचारणीय हैं- ‘हमारी आंखे अपनी होती हैं, किंतु देखते हैं दूसरों की नजरों से हमारे कान अपने होते हैं, कितु श्रवण-शक्ति दूसरों की हमारा मस्तिष्क अपना होता है, किंतु चिंतन-प्रणाली अन्य की। यदि आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो अपनी ज्ञानेन्द्रियों को गुलामी से छुड़ाइए-अपनी आंख से देखिए, अपने कान से सुनिए, अपनी नाक से सूंघिए, अपनी जीभ से चखिए। सोचिए अपने ढंग से, बोलिए अपनी बात।’ भाषा के संबंध में बेनीपुरी जी की ये पंक्तियां छोटे शहर के भाषा के वाहकों के लिए भी यह उतनी ही विचारणीय है जितनी की महानगरों के भाषा-भाषियों के लिए ।
एक प्रश्न यह भी सामने है कि ‘जो साक्षर हैं क्या वे ही भाषा के खेवनहार हैं?’ नहीं ऐसा कदापि नहीं है। बल्कि यह कहना अधिक तर्क संगत है कि निरक्षरों की भूमिका किसी भी भाषा के विकास में अधिक सार्थक रही है। निरक्षर का तात्पर्य अज्ञान से नहीं है। अकबर के संबंध में कही पढ़ा था कि अकबर साक्षर नहीं था। किंतु उसमें ज्ञान लिप्सा अधिक थी। वह पुस्तकें पढ़ तो नहीं सकता था परन्तु 1605 में उसके पुस्तकालय में 24000 चुनी हुई हस्तलिखित पुस्तकें मिली। वह बहुत सी पुस्तकों की दो-दो प्रतियां रखता था- एक प्रति बाहर रहती थी और दूसरी उसके अतःपुर में।
गढ़वाली में आज भी निरक्षरता का प्रतिशत है। किंतु निरक्षरों में भी ज्ञान लिप्सा की कमी नहीं है। यह लिखने में भी अतिशयोक्ति नहीं है कि गढ़वाली भाषा का बहुमूल्य खजाना ये निरक्षर ही हैं। गढ़वाली लोकभाषा है अथवा भाषा? यह न इनके दिमाग की उपज है और न कभी रही है। किंतु यदि यह कहना -लिखना ही जरूरी है तो निसंकोच कह सकते हैं कि गढ़वाली लोकभाषा भी है और भाषा भी है। लोक भाशा की यदि बात करें तो हमारे सम्मुख लोक विरासत का अथाह भण्डार सुरक्षित है।
गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य में डाॅ हरिदत्त भट्ट ‘शैलेश’ इसी ओर इंगित करते हुए लिखते हैं कि ‘आधुनिक युग में जनपद-साहित्य या लोक-साहित्य का महत्व सभी ने स्वीकार किया है। गढ़वाल जनपद के लोक गीतों, लोक कथाओं, लाकोक्तियों आदि के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए गढ़वाली का अध्ययन जरूरी है।’ अतः लोकभाषा अथवा लोक-साहित्य को सहेजने वाले भी साहित्यकार हैं और भाषा के रूप में उसे परिमार्जित करने वाले भी साहित्यकार ही हैं ।
लेकिन त्याग की भावना दोनों के लिए अपेक्षित है। वह कैसे? हिंदी भाषा की ख्यातनाम लेखिका महादेवी वर्मा से जुड़ा एक प्रसंग पढ़िए। उन्होंने लिखा है-
‘मेरा मन था, गांधी जी को अपनी कुछ कविताएं सुनाऊं, तो हमनें उन्हें बताया कि हम कविताएं लिखती हैं। उन्हें बताया कि एक कविता प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला है। आप भी हमारी कविताएं सुनिए। गांधी जी की आंखे चश्मे के पीछे से चमकी। वे बोले- कविताएं नहीं सुनूंगा। अलबता अपना चांदी का कटोरा मुझे दे दो। देश के काम आयेगा। हमनें कटोरा गांधी जी को दे दिया। और उनके पास से लौटते हुये प्रण किया कि अब कभी अपने मुंह से अपनी कविता किसी को नहीं सुनाएंगे।’ अब इसे त्याग कहें या यूं कहें ऐसी परिस्थिति में हम में से कितने लोग अपने कवच-कुंडल देने के लिए तैयार हैं?
कोई रचना या पुरस्कार देश से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन भाषा और देश दोनों में से किसी एक का चयन करने के लिए कहा जाय तो किसका चयन करें? आयरलैंड की गालिक भाषा से जुड़ा एक उदाहरण गणेश शंकर विधार्थी जी केे ‘अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन’ के 19 वे (गोरखपुर) अधिवेशन में 2,3,4, मार्च 1930 के अध्यक्षीय भाषण में पढ़ने को मिला है। जिसको की ‘भाषा बचेगी तो देश बचेगा’ के शीर्षक से ‘अक्षर पर्व’ ने अपने जून 2007 के अंक में स्थान दिया है।
विधार्थी जी के शब्द हैं- ‘भाषा संबंधी सबसे आधुनिक लड़ाई आयरलैंड को लड़नी पड़ी थी। पराधीनता ने गालिक भाषा का सर्वथा नाश कर दिया था। दुर्दशा यहां तक हुई कि इने-गिने मनुष्यों को छोड़कर किसी को भी गालिक का ज्ञान न रहा था, आयरलैंड के समस्त लोग यह समझते थे कि अंग्रेजी ही उनकी मातृभाषा है और जिन्हें गालिक आती भी थी, वे उसे बोलते लजाते थे और कभी किसी व्यक्ति के सामने उसके एक शब्द का भी उच्चारण नहीं करते थे। आत्मविस्मृति के इस युग के पश्चात आयरलैंड की सोती हुई आत्मा जागी, तब उसने अनुभव किया कि उसने स्वाधीनता तो खो ही दी,किंतु उससे भी अधिक बहुमूल्य वस्तु उसने अपनी भाषा भी खो दी।
गालिक के पुनरूत्थान की कथा अत्यंत चमत्कारपूर्ण और उत्साहवर्द्धक है। उससे अपने भाव और भाषा को बिसरा देने वाले समस्त देशों को प्रोत्साहन और आत्माद्धार का संदेश मिलता है। इस शताब्दी के आरंभ हो जाने के बहुत पीछे, गालिक भाषा के पुनरुद्धार का प्रयत्न प्रारम्भ हुआ। देखते-देखते वह आयरलैंड भर पर छा गई। देश की उन्नति चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति गालिक पढ़ना और पढ़ाना अपना कर्तव्य समझने लगा। सौ वर्ष बूढ़े एक मोची से, डी-वेलरा ने युवावस्था में गालिक पढ़ी और इसलिए पढ़ी की उनका स्पष्ट मत था कि यदि मेरे सामने एक ओर देश की स्वाधीनता रखी जाये और दूसरी ओर मातृभाषा और मुझे पूछा जाये कि इन दोनों में एक कौन -सी लोगे तो, एक क्षण के विलंब बिना मैं मातृभाषा को ले लूंगा।’
गढ़वाली भाषा पर गालिक भाषा की भांति अभी इतना आसन्न संकट भी नहीं है। और न ही कोई संत डी-वेलरा जैसे तपस्या रत है।
एक अन्य उदाहरण जापानी भाषा का मिला है। ‘भारत और मानव संस्कृति’ में विशम्भर नाथ पांडे ने जापानी भाषा के लेखक ‘कोबोदाइशी’ के योगदान का उल्लेख करते हुए लिखा है कि ‘कोबोदाइशी ने शिक्षा को सर्वसाधारण के लिए सुलभ कर दिया। उसने संस्कृत वर्णमाला के आधार पचास अक्षरों की जापानी वर्णमाला तैयार की और इन पचास अक्षरों में एक ऐसी कविता की रचना की जिसमें कोई अक्षर दोबारा प्रयुक्त नहीं हुआ। उस अद्भुत कविता को ‘इरोह’ कहते हैं। इस कविता की रचना में महापरिनिर्माण सूत्र से प्रेरणा मिली। प्रत्येक जापानी बालक को यह कविता मुखाग्र कराई जाती है।’ अभी गढ़वाली भाषा के कलमकारों की इस स्तर की योग्यता भी देखनी बाकी है।
क्या यह युक्ति सही नहीं है कि आज हम गढ़वाली भाषा को मात्र सुनने और सुनाने के दौर से गुजरते देख रहे हैं। प्रश्न विचारणीय है क्या गढ़वाली भाषा सुनने -सुनाने या तम्बू सामियाने तानने के लिए ही है? मेरी पुस्तकें मेरे बस्ते में हैं। आपकी आपके बस्तों में हैं। कुछ बस्ते ऐसे भी हैं जिन्हें ढोने वाले अब नहीं हैं। दम-खम्म से कहते तो हम सब हैं कि गढ़वाली भाषा की हर एक पुस्तक, हर एक बस्ता बहुमूल्य है। लेकिन विडम्बना देखिए हम गढ़वाली भाषा के 500 साल लम्बे इतिहास का उद्धरण देते हैं लेकिन…. हमारे पास अभी तक गढ़वाली भाषा का एक अदद पुस्तकालय तक नहीं है।
ऐसा नहीं है कि हम चूक गये हैं या अब समय नहीं है। आइये! सबसे पहले गढ़वाली को बोली, उपबोलियों के संकीर्ण क्षेत्रीय दायरों से मुक्त करें! एक पक्षीय नहीं, बहु पक्षीय चिंतन करें! अनमोल बस्तों की धूल-गर्द साफ करें! उन्हें शोध प्रबन्धन के लिए समुचित स्थान देने की पहल करें! साथ ही गढ़वाली ‘भाषा’ है! सचेतन सगर्व कहें!